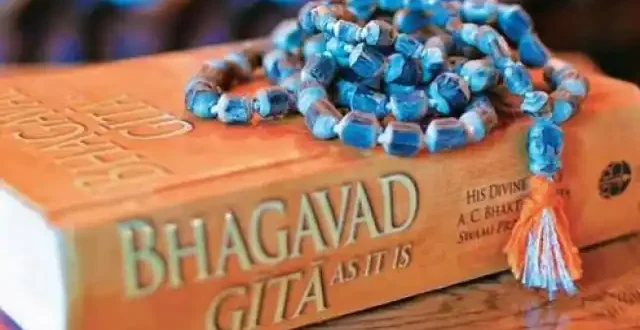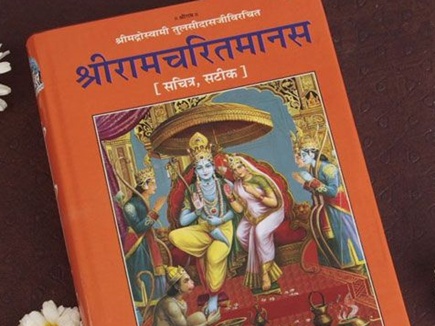
त्रेतायुग में रामायण काल में चरित्रों के माध्यम से जो आदर्श पहले क्रियान्वित किए गये जिनका वर्णन श्रीरामचरितमानस में हुआ उन्हीं आदर्शों का सार तत्व श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा गया। श्रीराम का राजनयिक प्रबंधन ही जीवन का सर्वस्व है।
हनुमान जी विद्वान हैं, गुणी हैं और चतुर हैं, पर उनकी विशेषता यह है कि वह चतुराई का उपयोग रामकाज के लिए करते हैं। उसी गुण का रोपण और जागरण भगवान श्रीराम ने बालिपुत्र अंगद में कर दिया था। लंका जाते समय अंगद के प्रोत्साहन के लिए कह दिया कि : “बहुत बुझाइ तुम्हहिं का कहहूं। परम चतुर मैं जानत अहहूं।।” मैं तो जानता हूं कि तुम परम चतुर हो, इसलिए तुम लंका जाकर ऐसा कार्य करना कि मेरा भी कार्य पूर्ण हो और रावण का भी हित हो। अब रावण के हित की परिभाषा कोई श्रीराम, हनुमान जी, और अंगद की अलग नहीं है। एक ही उद्देश्य और परिभाषा है कि रावण सीता जी को लौटा दे।
रामायण में भक्ति को मणि की उपमा दी गई है। राम नाम को भी मणि कहा गया है। भगवान स्वयं नीलमणि हैं। जो इसके मर्म को जान गया और जिसने इसकी खोज में अपनी चतुराई से इस प्रकाश के उपादान रहित परम प्रकाशमयी मणि को प्राप्त कर लिया, बस वही भक्त और ज्ञानी है। कर्मयोग भी उसी ने सिद्ध किया है। रावण और दर्योधन भी चतुर थे, पर वे दोनों मन, वचन, कर्म से चतुरता का उपयोग अपने निजी भोग और स्वार्थ के लिए करके चतुरता के गुण को दोष में बदल देते थे। इसीलिए गीता में अंतिम श्लोक में वेदव्यास ने कह दिया है कि जिधर श्रीकृष्ण होंगे और जिधर उनका भक्त अर्जुन होगा, वहीं पर संसार की सारी श्री विराजमान रहेगी। वहीं विजय होगी और वहीं पर ऐश्वर्य होगा। मेरी अचल नीति भी वहीं होगी। जैसे अंगद का पैर कोई हिला नहीं सका, वैसे मेरे भक्त के जीवन में कभी अनीति नहीं आ सकती है।
रामचरितमानस में भी कहा गया है : “भूमि न छांड़त कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।।” जहां सुनीति की अवहेलना होती है और सुरुचि को प्रमुखता दी जाती है, वहां पर व्यक्ति उत्तानपाद होकर पैर ऊपर कर लेता है और सिर नीचे कर लेता है। विवेकहीन के यही लक्षण होते हैं- विवेक अधोगामी और कर्म ऊर्ध्वगामी। सुरुचि के प्रति जब-जब हमारा आकर्षण होता है, तब तब सुनीति की अवहेलना हो जाती है। तब भगवान के भक्त ध्रुव की उपेक्षा होती है। चाहे ध्रुव हों, प्रह्लाद हो या भरत हों या अर्जुन, भगवान तो अपने भक्त के ही होते हैं। क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। जहां भगवान हैं, वहीं भक्त है। जहां भक्त हैं, वहीं भगवान हैं। “यत्र योगेश्वर:कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धु्र्वानितिर्मतिर्मम।।” विभीषण, माल्यवान, मंदोदरी सभी ने रावण को नीति का ही उपदेश दिया, पर रावण को तो सीता जी में सुरुचि दिखाई दे रही थी, अत: उसका तो उत्तानपाद होना निश्चित ही था। भगवान राम ही एक एक ऐसे अवतार हैं, जिनके जीवन में नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ का सामंजस्य है। परिपूर्णता है।
रावण के जीवन में प्रीति आगे होती है, पीछे नीति छिपी रहती है। रावण के जीवन में परमार्थ आगे दिखाई देता है और पीछे स्वार्थ छिपा रहता हैं, पर श्रीराम के जीवन में नीति आगे दिखाई देती है और प्रीति पीछे छिपी रहती है। स्वार्थ आगे दिखाई देता है और परमार्थ पीछे छिपा रहता है। यही नीति प्रधान और अनीति युक्त मानस का आंतरिक अंतर है। राम की नीति, प्रीति, परमार्थ प्राणी मात्र के कल्याण के लिए था, इसलिए राम की ही तरह राम के कार्य भी पूर्ण हैं। सबको जोड़ना ही उनका प्रबंधन है। दुर्योधन के साथ कर्ण का होना तथा रावण के साथ मेघनाद का होना ही उन दोनों के विनाश का कारण बना। दूसरी ओर विभीषण के साथ राम का होना और अर्जुन के साथ कृष्ण का होना ही परमार्थ बन गया।
वस्तुत: गीता और रामायण तो एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। अंतर केवल इतना है कि गीता में बीज हैं, रामायण में उन्हीं बीजों के वृक्ष और फल हैं। जब कोई उपदेश पात्रों के जीवन में घटित दिखाई देता है तो वह समझने और ग्रहण करने में अधिक सुगम हो जाता है। विभीषण और अर्जुन ऐसे दो पात्र हैं, जो दोनों अवतारों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विभीषण से भगवान राम ने कहा, “तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौं देह नहिं आन निहोरे।।” सगुण साकार ईश्वर की उपासना की पृष्ठभूमि और आधार बताते हुए श्रीराम विभीषण से कह देते हैं कि मेरे जो भक्त हैं, वे परहित की भावना ही उनमें प्रबल होती है, क्योंकि मेरे किसी रूप विशेष की पूजा वस्तुत: मेरी वास्तविक पूजा नहीं है। सारे संसार में मुझे देखना और सबके हित की भावना करना ही मेरी पूजा है। गीता में अर्जुन से भी वही कहा कि, “सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, मत्त:स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम्।।” सारा संसार और सब प्राणियों में मैं ही हूं, इसलिए मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। जो सृष्टि के किसी पदार्थ या प्राणी में मुझसे अलग कुछ भी देखता है, वही माया या अविद्या है, जो मनुष्य को भवसागर रूप अज्ञान में डुबा देती है। समस्त वेदों में मेरी ही उपासना का विधान है, चाहे वह कर्म मार्ग हो, भक्ति या ज्ञानमार्ग हो।
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सब मैं ही हूं। श्रीराम ने विभीषण को उपदेश में भी इसी तरह की बात कही है कि संसार के सारे संबंधों को मेरे चरणों से बांध दो तो उसका लाभ तुम्हें यह मिलेगा कि मैं बंध जाऊंगा और तुम मुक्त हो जाओगे : जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मनहिं बाँधु बर डोरी। पर संसार के लोग क्या कहें? कि संसार से संबंध बनाकर बंध जाते हैं और फिर मुक्ति की बातें क
 Govardhan Times | गोवर्धन टाइम्स Hindi News Portal & NewsPaper
Govardhan Times | गोवर्धन टाइम्स Hindi News Portal & NewsPaper